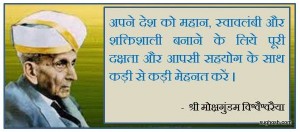उदयपुर शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, झीलों, बाग-बगीचों, शौर्यपूर्ण इतिहास, विशिष्ठ शिल्प शैली और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिये विश्व प्रसिद्ध है । वास्तविकता यह है कि आज भी जो पर्यटक आते हैं वे यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य और यहाँ की स्थानीय शैली में निर्मित पुराने भवन, बिना बिजली के चलने वाले फव्वारे, झरोखे, गोखडे़ आदि देखने में रुचि रखते हैं न कि नव निर्मित कॉम्प्लेक्सों या बंगलों को । ऐसे शीशे लगे बहुमंज़िले भवन तो हम से कहीं अच्छे विदेशों में हैं । हमारा अतीत बहुत गौरवमय रहा है और अगर हम स्मार्ट सिटी बनने की ललक में हमारा अतीत नहीं संभाल पाए तो यहाँ का आकर्षण ही समाप्त हो जायगा ।
यदि हम उदयपुर की पुरानी बसावट का विवेचन करें तो यह पाएंगे कि हमने एक विलक्षण विरासत पाई है जिसे साकार रूप देने वाले स्थानीय लेकिन कम पढ़े लिखे गुणीजनों के सामने आज के उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पर्यावरणविद् और कन्सल्टैंट बिल्कुल बौने हैं। तत्कालीन नियोजक यह जानते थे कि पानी, पत्थर या रेत आदि की तुलना में बहुत देर से गर्म होता है और उतनी ही देर से ठंडा होता है इसलिये यदि नगर के पास प्रचुर मात्रा में सतही जल हो तो समुद्र के किनारे की तरह दिन और रात के तापमान में अंतर कम रहेगा और मौसम सम-सीतोष्ण रहेगा । वे यह भी जानते थे कि हरियाली हवा को गर्म नहीं होने देती है और उसमें नमी बनाए रखती है जिससे मौसम तरोताज़ा रहता है और पेड़ हवा की गति को शिथिल करते हैं जिससे आँधी चलने की संभावना घटती है । वे यहाँ की हवाओं का रुख भी जानते थे जो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। इन सब को ध्यान में रख कर उन्होंने नगर के दक्षिण पश्चिम में विशाल आकार की झीलें बनाईं और उत्तर पूर्व में फतहसागर की नहरों से सिंचित होने वाला लगभग 1000 एकड़ का हरा भरा सिंचित क्षेत्र रखा । नगर के बाहर तो जंगल थे ही, उन्होंने आठ किलोमीटर लंबी शहरकोट से धिरे नगर के अंदरूनी 3.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 16 प्रतिशत भाग मे सघन प्राकृतिक वन और इतने ही भाग में बाग-बगीचे बनाए । इसकी वजह से हमारे यहाँ गर्मियों में गर्मी कम और सर्दियों में सर्दी कम लगती थी, रात और दिन के तापमान में अंतर कम रहता था और आँधियां कभी कभार ही चलती थीं । घने जंगलों और हरियाली की वजह से वर्षा भी पर्याप्त होती थी जिससे यहाँ की झीलों के नाले एक एक माह तक चलते ही रहते थे। आज आबादी तो सात गुनी हो गई है लेकिन गुलाब बाग सात नहीं हुए हैं और हरे भरे क्षेत्र तो नाम मात्र के रह गए हैं क्योंकि लगभग सारा कृषी क्षेत्र नव विकसित कॉलोनियों की चपेट में आ चुका है।
हमारे पुरखे यह भी जानते थे कि मानसूनी प्रकृति के कारण वर्षा में वर्ष दर वर्ष भारी अंतर रहना निश्चित है और कभी एक साथ दो साल अतिवृष्टि के तो कभी एक साथ दो साल अनावृष्टि के हो सकते हैं। इसलिये उन्होंने झीलों की जल संग्रह क्षमता औसत जल आवक की तीन से पाँच गुनी निर्धारित करने की नीति अपनाई जिससे अतिवृष्टि वाले वर्ष का पानी भी संग्रहित हो और अनावृष्टि के वर्ष में काम आ सके। आज के विशेषज्ञ बाँध की लागत घटाने के लिये औसत जल आवक की तीन चैथाई जल संग्रह क्षमता ही रखने का सिद्धांत अपनाते हैं जो यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है । उपलब्ध जल का दक्षतम उपयोग हो इसके लिये उन्होंने संग्रहित पानी को पहले सिंचाई के काम में लेने और सिंचाई के दौरान रिसे पानी को कुओं वावड़ियों से खींच कर पेयजल के काम में लेने की नीति रखी जिसके अंर्तगत गुलाबबाग और सहेलियों की बाड़ी जैसे सिंचित क्षेत्र में कुएं और बावड़ियाँ बनवाईं । इस प्रणाली से नगर के पास ही अनाज, सब्जी और आम अमरूद जैसे फल तो खूब हो ही जाते, हरियाली भी बनी रहती थी । आज हम झीलों के पानी को सीधा पेयजल के काम लेते हैं जिससे इसके उपयोग की दक्षता तो घटी ही है, हरा क्षेत्र भी घट गया है और भूजल का स्तर भी नीचे चला गया है।
तत्कालीन गुणीजन वाष्पीकरण हानि को कम करने की तकनीक से भी परिचित थे जिन्होंने झीलों के पानी को रबी फसल में सिंचाई के काम में लेने की नीति रखी जिससे झीलों का जल स्तर गर्मी आते आते नहर तल तक आ जाता था और जल का फैलाव सीमित हो जाता था। सीमित फैलाव से वाष्पीकरण हानि कम हो जाती थी। रबी की सिंचाई से भू जल का पुर्नभरण भी भरपूर होता और सिंचाई के शेष पानी के निकास से आयड़ नदी में भी कुछ न कुछ बहाव बना ही रहता था । पेयजल के लिये पानी सीधा झीलों से न ले कर सिंचित क्षेत्र के मध्य निर्मित कुओं और बावड़ियों से लिया जाता था जहाँ पानी अपेक्षाकृत रूप से शुद्ध होता था और इससे शुद्धिकरण में लगने वाला खर्चा कम होता था । उन दिनों दिन में दो बार नल आते थे और प्रेशर भी पूरा रहता था। सार्वजनिक नल भी लगभग हर मौहल्ले में थे। इस कारण निजी ट्यूब वैलों पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी।
झील संरक्षण बिना लागत के स्वतः करने में भी तत्कालीन नियोजक निष्णात थे। प्रथमतः तो उन्होंने झीलों का मोरी तल ही इस प्रकार निर्धारित किया कि लगभग आधी भराव क्षमता नहर तल से नीचे रहे और काम में न ली जा सके। उदाहरण के लिये फ़तहसागर में कुल 33 फुट गहराई में से नहर तल 13 फुट पर है शेष 20 फुट गहराई का पानी मूल डिज़ाइन के अनुसार रिज़र्व (डैड स्टोरेज) है। आज के विशेषज्ञ कुल क्षमता का 10 प्रतिशत ही रिज़र्व डैड स्टोरेज रखते हैं जबकि हमारे पुरखे 50 प्रतिशत रिज़र्व डैड स्टोरेज रखा करते थे। आज हम उनके द्वारा निर्धारित रिज़र्व डैड स्टोरेज को भी पंप करके झीलों का पैंदा निकालते रहते हैं जिससे मछलियाँ समाप्त हो जाती हैं और झीलें कभी कभी ही ओवरफ्लो हो पाती हैं। ये परिपाटी इन झीलों की दुर्दशा का मुख्य कारण है । पुरानी प्रणाली में झीलों का पैंदा निकलने की नौबत ही नहीं आती थी जिससे इसमें पर्याप्त और बड़ी बड़ी मछलियाँ सदा ही रहती थीं जो जल को शुद्ध रखने में सक्षम थीं । उस समय हालत यह थी कि अगर आपके पाँव में फोड़ा हो रहा है और आपने पानी में अपना पैर रख दिया तो मछलियाँ तत्काल आ कर उस फोड़े का पीप चट्ट कर जातीं साबुन की बट्टी पानी में गिरने पर वह तत्काल मछलियों का भोजन बन जाती थी । इस रिजर्व पानी की पूर्व उपलब्धता के कारण बरसात में सामान्य सी वर्षा होने पर भी झीलें पूरी भर जातीं और नाला चलने से पानी पलटा हो जाता था । इस कारण कितने ही लोग रोज़ इन झीलों में नहाते धोते फिर भी पानी साफ़ ही रहता था। आज हम मछलियाँ बचाने और बढ़ाने की नहीं, नहाने धोने पर रोक लगाने की तरफदारी कर रहे हैं।
सरकारी खर्चे से सिल्ट निकालने का रिवाज़ उन दिनों नहीं था क्योंकि इसे ईंटे, केलू आदि बनाने के लिये कुम्हार और खेतों में पणे के रूप में काम में लेने के लिये काश्तकार खुद ही साल दर साल ले जाते रहते थे। उल्टे पाबंदी यह थी कि सिल्ट (पणा) केवल वरावले (मुहाने) से ही निकाला जावे जो पीछोला मे सिसारमा के पास और फतेहसागर में नीमचमाता के पास रानी रोड के मोड़ पर था । इससे झीलों का पैंदा उघड़ने के कारण रिसाव बढ़ने की आशंका भी नही रहती थी और अगले साल बरावले में ही, जहाँ पानी का वेग रुकता है, सिल्ट वापस जमा मिलती थी जिसे आसानी से निकाला जा सकता था। आज ये पणा काश्तकारों द्वारा कम और वाटिकाओं व रिसोर्टो के मालिकों द्वारा ज्यादा काम में लिया जाने लगा है इसलिये ये कोई न कोई कारण बना कर सरकारी खर्चे से इसे निकलवाते हैं बाकी अंतिम उपयोग तो पुराना ही है।
हमारे पुरखों ने आबादी क्षेत्र के लिये अनुपजाऊ पहाड़ी क्षेत्र चुना जो यहाँ के महलों, जगदीश मंदिर, गणेश घाटी, मेहताजी का टिम्बा आदि की स्थिति से स्पष्ट है । उपजाऊ भाग को उन्होंने कृषी कार्य के लिये छोड़ दिया था ताकि नगर में ग्रीन बेल्ट प्रचुर रूप में रहे। नगर में मार्ग यद्यपि संकड़े थे जो तत्समय की सुरक्षा आवश्यकताओं और यातायात के साधनों को देखते हुए पर्याप्त थे लेकिन वैकल्पिक मार्ग व क्रोस कनेक्शन इतने अधिक थे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अनावश्यक दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी । जगह जगह पर नोहरे और चौक थे जो आज भी सामुदायिक कामों के लिये बहुत उपयुक्त हैं । दुकानें केवल भूतल पर ही थी जिनके आगे पतला बरामदा हुआ करता था । पहली मंज़िल बरामदे को छोड़ कर शेष भाग में बनाई जाती थी जिससे सड़क पर धूप हवा और रोशनी पूरी रहे और ऊपर रहने वालों को भी बरामदे की खुली छत पर धूप और हवा मिल सके। हर घर के बाहर एक चबूतरी और बीच में एक खुला चौक होता था जिसका फर्श अधिकतर कच्चा ही होता था। इससे निवासियों को धूप और हवा पूरी मिल जाती थी। खुले चैक में तुलसी, केले आदि के पौधे लगे होते थे जो वातावरण को शुद्ध बनाते और भू जल का पुर्नभरण भी स्वतः ही हो जाता था। जगह जगह धर्म स्थल थे जहाँ बुज़ुर्ग लोग एकत्रित हो कर आपस में दुःख सुख की बातें कर अपना जी हल्का कर सकते थे। आज भी श्री जगदीश मंदिर जैसी जगहों पर यह स्थिति देखी जा सकती है। हमारी आधुनिक नव विकसित कॉलोनियों में भव्य इमारतें हैं लेकिन ये सब सुविधाएं नहीं के बराबर हैं।
नगर का विकास हमने निजी डवलपर्स के भरोसे छोड़ दिया है जो सस्ते में कृषी भूमि खरीद कर उसमें कम से कम सुविधा क्षेत्र छोड़ते हुए अधिक से अधिक भू भाग बेचने के प्रयास में रहते हैं। टुकड़े टुकड़े में कट रही कॉलोनियों में एक दूसरे से लिंक नहीं रहता है और डैड एंड की भरमार है। ठीक पास के या पीछे के प्लॉट में जाने के लिये भी आपको लंबा चक्कर काटना पड़ सकता है और एक जगह रास्ते में कोई बाधा आ जाय तो वैकल्पिक मार्ग ही नहीं मिले ऐसा भी हो सकता है। अधिकांश प्लॉट मालिक यह धारणा रखने लगे हैं कि प्लॉट में खुला स्थान छोड़ना मूर्खता है । तथाकथित आर्किटैक्ट अपना बिज़नेस न गंवाने के चक्कर में भवन निर्माता को खुले स्थानों की उपयोगिता का तकनीकि आधार ही प्रकट नहीं करते हैं । बाउंड्री से बाउंड्री तक निर्माण करना और अधिक से अधिक प्रोजेक्शन निकालना आज भवन निर्माता की प्रतिष्ठा का मापदंड बन गया है। भवन की सुरक्षा और भूकंप के दौरान स्थायित्व के लिये यह ज़रूरी है कि मंज़िल दर मंज़िल निर्मित क्षेत्र घटे यानि कि भवन पिरामिड आकार का हो लेकिन आज आर सी सी निर्माण प्रक्रिया का दुरुपयोग कर हम ऊपर की मंज़िलों में निर्मित क्षेत्र नीचे की मंज़िलों से भी अधिक रखने लगे हैं।
विकास के मायने यह हो रहे हैं कि सड़क का कोई भी भाग कच्चा न रहे उस पर डामर या फिर सीमेंट कंक्रीट हो । इससे बरसाती पानी जमीन में नहीं समा पाता और सड़कें ही दरिया बन जाती हैं। चाहे प्लॉट के अंदर हो या सड़क पर, हज़ारों वर्गमीटर भू सतह को भारी खर्च कर पहले तो हम कंकरीट या डामर से जल रोधी बना कर भू जल का प्राकृतिक पुर्नभरण रोकने का पक्का इंतज़ाम करते हैं फिर कुछ भवनों की कुछ वर्गमीटर छतों का पानी पाइपों के माध्यम से विद्यमान ट्यूब वैल में डालने का “वाटर हारवेस्टिंग” कानून बना कर भू-जल के पुर्नभरण का टोटका करते हैं ।
आर सी सी के बजाय पत्थर के छज्जे बनाने, घर के अंदर कुछ न कुछ कच्चा भाग छोड़ने, अपनी सीमा के बाहर सड़क की ओर प्रोजेक्शन न निकालने, पहली मंजिल के बाद सड़क की ओर बढ़ने के बजाय कुछ खसका छोड़ने जैसी पुरानी परम्पराएं हमें वापस अपनानी होंगी ।
हमने उदयपुर के मूल स्वरूप के साथ जम कर खिलवाड़ किया है और हमारे पुरखों की दूरदर्शिता से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। यहाँ पर ‘‘घर का जोगी जोगणा और आन गाँव का सिद्ध‘‘ की कहावत पूरी तरह से चरित्रार्थ हो रही है। बाहर से आये कन्सल्टैंट लाखों की फीस ले जाते हैं और ऊपरी आंकड़ों पर आधारित ऐसी कागज़ी योजना हमारे हाथों में थमा जाते हैं जिनकी रिपोर्ट और उसकी साज सज्जा केवल देखने में ही सुंदर होती है, अंदर ज्यादातर कॉपी पेस्ट ही होता है। ऐसी अव्यावहारिक योजनाओं के क्रियान्वन से खर्चा तो खूब हो जाता है लेकिन परिणाम शून्य, अल्पकालीन या ऋणात्मक रहता है। विकास कार्यों का क्रियान्वन ऐसे हाथों में है जिन्हें उदयपुर से कोई लगाव नहीं है और न कोई जबाबदेही है । इस सब के चलते विकास की आँधी में हम उदयपुर की पहचान खोते जा रहे हैं। यहाँ का विशाल काँचों वाला नवनिर्मित एयरपोर्ट भवन उदयपुर का नहीं बल्कि किसी विदेशी शहर का एयरपोर्ट लगता है। रेल्वे स्टेशन पर बनी होटल पर जो छज्जे निकाले गए हैं वो झुकी मूँछ जैसे लगते हैं जो मेवाड़ी आन बान के पूरी तरह विपरीत हैं ।
नागरिक इस स्थिति के या तो मूक दर्शक हो रहे हैं या फिर इतना सोचने की उन्हें फुर्सत ही नहीं है। यह एक चेतावनीपूर्ण स्थिति है। ज़रूरी है कि हम समय रहते चेतें व स्थिति को और बिगड़ने से रोकें । हमें उदयपुर के अतीत से शिक्षा लेनी होगी, विकास कार्यों को स्थानीय ढांचे में ढ़ालना होगा और स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना होगा ।
विकास कार्यों के निर्देशन के लिये स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों का एक नियंत्रण मंडल हो, बाहरी कन्सल्टेंटों की रिपोर्टों पर टिप्पणी के लिये संबंधित विषय के ज्ञाताओं की एक अधिकार प्राप्त तकनीकि समिति हो, सभी झीलों का कोई एक ही धणी धोरी विभाग या संस्था हो, नगर का विस्तार कृषी योग्य भूमि को लीलने से नहीं हो, स्थानीय शैली के पुरा-निर्माण संरक्षित हों और पुर्ननिर्माण या नव निर्माण भी स्थानीय शैली का पुट लिये हुए हों, भवनों के साथ पर्याप्त हरे और खुले क्षेत्र हों, सड़कों के डिवाइडर हरी झाड़ियों के हों, सड़कों के दोनों तरफ अनिर्बाधित फुट पाथ व पेड़ों की क्षंखला हो, पत्थरों की बाउंड्री वॉल्स के बजाय हरी कांटेदार हैज लगे, ऑटो रिक्शा व सिटी बसें सी एन जी से चलें, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुचारु हो, पार्किंग की अच्छी व पर्याप्त व्यवस्था हो, जैसे कई कदम उठाने उदयपुर के मूल गौरव, धरोहर व पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक हैं ताकि इसकी पहचान बनी रहे । इसके लिये जन जन को अपने से पहले उदयपुर के लिये समर्पित होना होगा व अपनी जड़ता छोड़नी होगी ।
– ज्ञान प्रकाश सोनी,
21 – सी, यशविहार,
फतेहपुरा, उदयपुर
94141 65520